पंकज शर्मा / वरिष्ठ पत्रकार


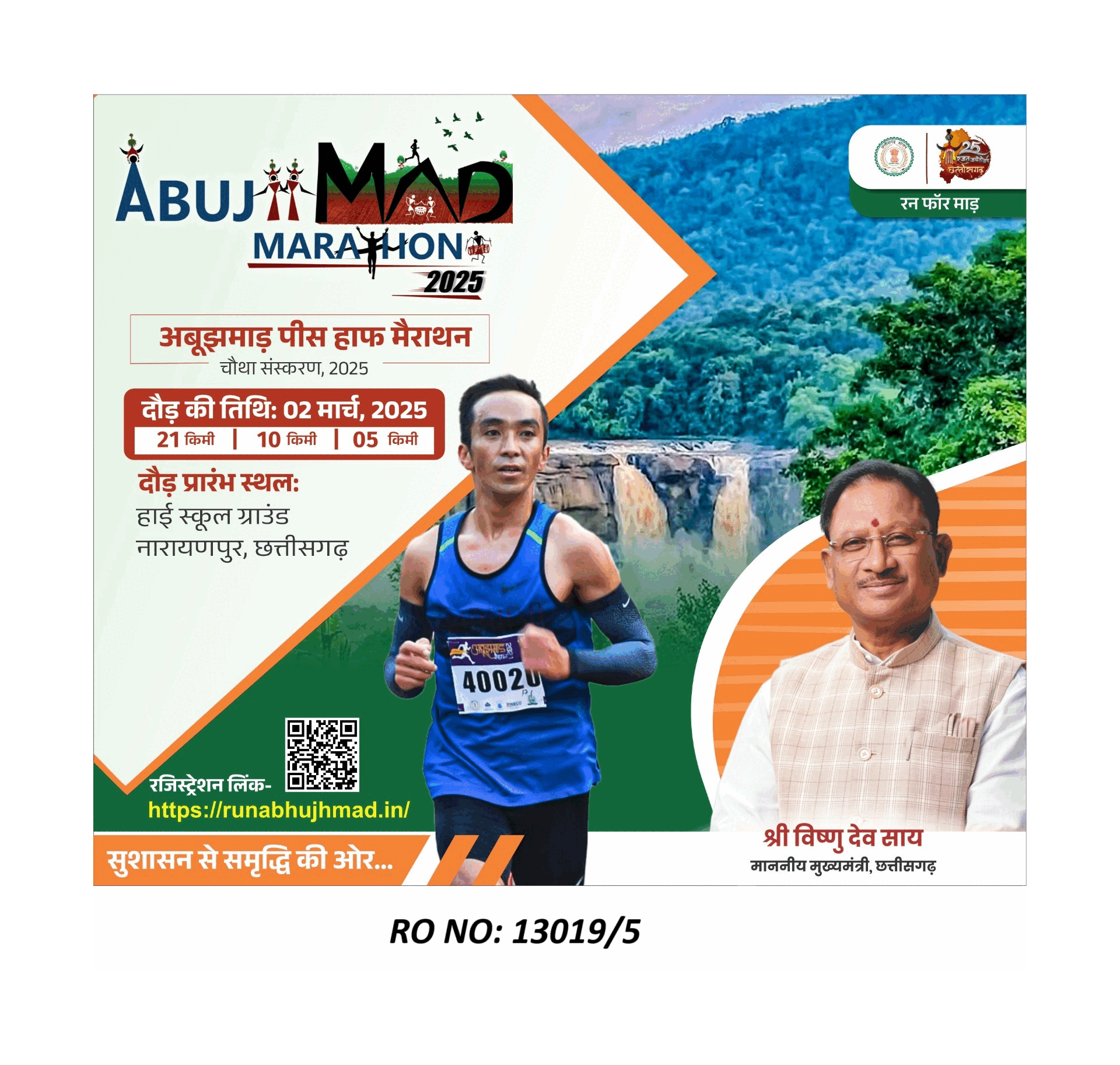
तो राजनीति अगर शुद्ध-सेवा है और अगर हमारे राजनीतिक इस पवित्र भाव में सराबोर हो कर सेवक बनने की होड़ में लगे हैं तो फिर तो भारत-भूमि धन्य-धन्य है कि हमें ऐसे जन-प्रतिनिधि मिले हैं। हम भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे राजनीतिक दल मिले हैं और उन राजनीतिक दलों के ऐसे आलाकमान मिले हैं, जो सुनिश्चित करते हैं कि हर चुनींदा सहयोगी को बारी-बारी से सेवा का मौका मिले। सबको बराबरी के अवसर देने का धर्म निभाने के लिए उनका अभिनंदन होना चाहिए।
लोकतंत्र में जन-निर्वाचन के ज़रिए चुन कर आए सेवा-उद्यत प्रतिनिधियों की दो टोलियां अपने-अपने मुखियाओं को कबीले की सल्तनत की देने का दबाव बनाएं तो इसे हम कैसा लोकतंत्र कहेंगे? दोनों मुखिया अपने-अपने योगदान गिनाएं और एक-दूसरे को सेवा का अवसर न दिए जाने की बिसात बिछाएं तो इसे हम कैसा जनतंत्र कहेंगे? पांच बरस की हुकूमत में दोनों को आधे-आधे वक़्त मुख्यमंत्री बनाने के समझौता-प्रयास करने पड़ें तो इसे हम कैसा प्रजातंत्र कहेंगे?
हालांकि पूरा नहीं आता, लेकिन यह तो फिर भी मेरी समझ में थोड़ा आता है कि दो योद्धा और उनके घुड़सवार युद्ध के बाद जीते गए राज में अपनी-अपनी कुर्बानियों का हिस्सा मांगें। लेकिन इससे ज़्यादा लज्जाजनक मुझे और कुछ नहीं लगता कि वे आधी-आधी अवधि के लिए हुक़्मरान बनने का सौदा करें। आख़िर वे तीस-तीस महीनों के लिए किसी एक प्रदेश का मुखिया बनना क्यों चाहते हैं? जन-सेवा किए बिना एक भी दिन उनसे रहा क्यों नहीं जा रहा है?
हमारी दुनिया में चिकित्सा-नर्स को सेवा का संभवतः सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। क्या आपने किसी मरीज़ की सेवा करने के लिए दो नर्सों में कभी इस तरह आपस में ठनते देखी है? क्या वे आधे-आधे समय किसी रोगी की तीमारदारी करने के लिए ऐसे ‘पहले मैं-पहले मैं’ करती हैं? बहुत-से डॉक्टर ज़रूर मरीज़ का इलाज़ करने की हवस लिए फिरते आपको दिख जाएंगे। वे ज़रूर ज़्यादा-से-ज़्यादा वक़्त अपने हाथ आए रोगी पर हाथ आजमाते रहने की तिकड़में करने में लगे रहते हैं और उसे अपने चंगुल से बाहर नहीं जाने देने की हर जुगत भिड़ाते हैं। लेकिन शुद्ध-सेवा में लगी नर्सों में यह होड़ मैं ने तो कभी नहीं देखी।
तो राजनीति अगर शुद्ध-सेवा है और अगर हमारे राजनीतिक इस पवित्र भाव में सराबोर हो कर सेवक बनने की होड़ में लगे हैं तो फिर तो भारत-भूमि धन्य-धन्य है कि हमें ऐसे जन-प्रतिनिधि मिले हैं। हम भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे राजनीतिक दल मिले हैं और उन राजनीतिक दलों के ऐसे आलाकमान मिले हैं, जो सुनिश्चित करते हैं कि हर चुनींदा सहयोगी को बारी-बारी से सेवा का मौका मिले। सबको बराबरी के अवसर देने का धर्म निभाने के लिए उनका अभिनंदन होना चाहिए।
मेरी इन बातों को कर्नाटक के संदर्भ में देख कर फूले नहीं समा रहे ख़ुराफ़ातियों से मैं कहना चाहता हूं कि भारत की समूची सियासत, सारे सियासी दलों और उनके तमाम आलाकमानों पर लानत भेजते हुए मैं भारी दिल से यह सब कह रहा हूं। सत्ता की बंदरबांट में अथाह दिलचस्पी आख़िर क्यों होती है, कौन नहीं जानता? प्रधानमंत्री बनने और बने रहने के लिए किसी भी स्तर तक उतर जाने के पीछे के कारण किसे नहीं मालूम हैं? क्यों कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है और आधे समय के लिए बनना हो तो पहले ख़ुद क्यों बनना चाहता है, इसका रहस्यलोक क्या इतना अबूझा है? यह किसी एक पोखर के पानी की सड़न का सवाल नहीं है, यह हमारे पूरे राजनीतिक तालाब से बेरतह उठ रही सड़ांध का बीज-प्रश्न है।
अगर लोकतंत्र का सारा कर्मकांड इसी व्यवस्था की जड़ों को सींचने के लिए होता है तो आप ही बताइए कि ऐसे लोकतंत्र को हम हार-फूल क्यों पहनाएं? क्या इससे बेहतर यह नहीं है कि हम उस पर हार-फूल चढ़ा दें? इसी व्यवस्था से जन्म लेने वाला और इसी व्यवस्था को पालने-पोसने वाला लोकतंत्र हमें चाहिए ही क्यों? क्या इसलिए कि उसमें अभिव्यक्ति की कथित आज़ादी मिलने का आभास हम में बना रहता है? क्या इसलिए कि उसमें अपने विधायिका-प्रतिनिधि ख़ुद चुनने का आभास हम में बना रहता है? क्या इसलिए कि उसमें जनतंत्र की खुली हवा में सांस लेने के श्रेष्ठि-भाव का आभास हम में बना रहता है? लेकिन यह आभासी संसार कितना नकली है, यह हम से बेहतर कौन जानता है?
सो, भीतर से बुरी तरह पिलपिली हो गई इस व्यवस्था को बदलने की इच्छा और हिम्मत अगर नरेंद्र भाई मोदी में नहीं है और राहुल गांधी इसकी ख़्वाहिश और साहस रखने में मजबूर हैं तो लोकतंत्र के नाम पर एक ऐसी व्यवस्था को अपने कंधों पर ढोते रहने का पाप जनता-जनार्दन भी क्यों करे, जो अवाम के ही बुनियादी हितों की धज्जियां बिखेर रही हो? जब हमें अंततः दुःख ही भोगने हैं तो हमारे नाम पर कोई दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का निर्वाचित मुखिया होने का सुख आख़िर क्यों भोगे?
किसी को देश-प्रदेश का मुखिया बनना है, बन जाए; मगर छीना-झपटी से ही बनना है तो खुलेआम बने। लोकतंत्र का बहाना लेकर न बने। धन के दबाव से, बल के दबाव से, जिस भी दबाव से बनना है, बन जाए, जनतंत्र का नाम कलंकित न करे। जब राजनीतिक दलों को चुनावों में उम्मीदवारों के नाम अन्यान्य आधारों पर ही तय करने हैं, जब उम्मीदवारों को चुनाव जीतने के लिए वही हथकंडे अपनाने हैं, जब चुनाव जीतने वाले दल को सरकार बनाने के लिए वैसी ही उठापटक करनी है और जब सरकारों को सेवा-समूह के बजाय उगाही-गिरोह की तरह ही काम करना है तो यह सब बेबस प्रजातंत्र की ओट में क्यों हो?
इससे तो अच्छा है कि हम किसी अधिनायक-राज में रहने का काला टीका माथे पर लगा कर खुलेआम घूमें। खुल कर घोषणा करें कि हां, हम अपने सुल्तानों के गुलाम हैं। और, हमारे हुक़्मरान भी अपने माथों पर इस श्याम-तिलक की छाप लिए विचरें कि वे निर्वाचित नहीं, एकाधिकारी शासक हैं। जब जनता की छाती पर उन्हें अपनी राजनीतिक मूंग दलनी ही है तो फिर जनता उनकी पगड़ी में लोकतंत्र का हीरा अपने हाथों क्यों टांके? लोकतंत्र का यह आवरण हुक़्मरानों से छिन जाए तो उनकी नंगई कम-से-कम दुनिया के सामने तो आए। हम-आप कब तक उनके नाखूनों और दांतों की ढाल बने रहें?
इसलिए या तो जनतंत्र के जन, प्रजातंत्र की प्रजा और लोकतंत्र का लोक अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों को व्यवस्था के बुनियादी बदलाव के लिए विवश करे या फिर दासप्रथा की वापसी का ऐलान कर दे। जब असलियत सब जानते हैं तो बेकार के ढकोसलों में क्या रखा है? दरअसल लोकतंत्र से किसी को कोई लेनादेना नहीं है। लोकतंत्र का तो सिर्फ़ नाम लिया जाता है। लोकतंत्र होता तो क्या एक-दो धनपशु इस तरह पूरे देश पर कब्जा कर पाते? लोकतंत्र होता तो क्या संवैधानिक संस्थाएं इस तरह चूं-चूं का मुरब्बा बन जातीं? लोकतंत्र होता तो हर हाल में सत्ता हड़पने की बढ़ती मारामारी के कुत्सित दृश्य क्या हम इस तरह देख रहे होते? लोकतंत्र होता तो फ़िजूल के बहाने बना कर किसी की संसद सदस्यता ऐसे ख़त्म हो जाती?
सो, यह मानने में कैसी हीन भावना कि जो है, उसे हम लोकतंत्र नहीं कह सकते। लोकतंत्र की यह अफ़ीम चाट-चाट कर हमारी ख़ुमारी इतनी बढ़ती जा रही है कि हम किसी काम के नहीं रह गए हैं। सिर्फ़ इस तरंग में मस्त हैं कि हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, हमारा लोकतंत्र सबसे जीवंत है, हमारा लोकतंत्र हमारी आन है, बान है, शान है। दिल-ही-दिल मे ंहम सभी जानते हैं कि दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोकतंत्र की जिस झीनी खटिया पर मस्ती से लेटे हुए हैं, उसके चारों पाए सफेद चींटी कब की चाट चुकी है। इन पायों के भुरभुरेपन को रोकना इस सफेदपोशी व्यवस्था से बाहर आए बिना अब मुमकिन नहीं है। यह बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए, अच्छा है।